- भ्रष्ट व्यक्तियों को अपर्याप्त सज़ा के कारण दंड से मुक्ति की धारणा भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दे सकती है। भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों को जब यह विश्वास हो जाता है कि वे दंड से बच सकते हैं, तो उनके इसमें शामिल होने की संभावना अधिक हो जाती है।
- भारत का जटिल आर्थिक वातावरण, जिसमें विभिन्न लाइसेंस, परमिट और अनुमोदन शामिल हैं, भ्रष्टाचार के अवसर पैदा कर सकते हैं। व्यवसाय इस माहौल से निपटने के लिये रिश्वतखोरी का सहारा ले सकते हैं।
सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार की व्यापकता के कारण:
- सिविल सेवा का राजनीतिकरण: जब सिविल सेवा के पदों का उपयोग राजनीतिक समर्थन के लिये पुरस्कार के रूप में किया जाता है या रिश्वत हेतु स्थानांतरण किया जाता है, तो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के अवसर काफी बढ़ जाते हैं।
- निजी क्षेत्र की तुलना में कम वेतन: निजी क्षेत्र की तुलना में सिविल सेवकों का वेतन कम हो सकता है, वेतन में अंतर की भरपाई के लिये कुछ कर्मचारी रिश्वत का सहारा लेते हैं।
- प्रशासनिक देरी: फाइलों की मंज़ूरी में देरी भ्रष्टाचार का मूल कारण है क्योंकि आम नागरिकों को फाइलों की शीघ्र मंज़ूरी के लिये दोषी अधिकारियों और प्राधिकारियों को रिश्वत देने को मजबूर होना पड़ता है।
- चुनौती रहित सत्ता की औपनिवेशिक विरासत: सत्ता के उपासक वाले समाज में सरकारी अधिकारियों के लिये नैतिक आचरण से विचलित होना आसान होता है।
- कानून का कमज़ोर प्रवर्तन: भ्रष्टाचार की बुराई को रोकने के लिये कई कानून बनाए गए हैं लेकिन उनके कमज़ोर प्रवर्तन ने भ्रष्टाचार को रोकने में बाधा के रूप में काम किया है।
भ्रष्टाचार का प्रभाव:
- लोगों और सार्वजनिक जीवन पर:
- सेवाओं में गुणवत्ता की कमी: भ्रष्टाचार वाली प्रणाली में सेवा की कोई गुणवत्ता नहीं होती है।
- गुणवत्ता की मांग करने हेतु किसी को इसके लिये भुगतान करना पड़ सकता है। यह कई क्षेत्रों जैसे- नगर पालिका, बिजली, राहत कोष के वितरण आदि में देखा जा सकता है।
- सबूतों की कमी या यहाँ तक कि मिटाए गए सबूतों के कारण किसी अपराध में संदेह का लाभ उठाया जा सकता है।
- इन निम्न-गुणवत्ता वाली सेवाओं का कारण इसमें शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीके से धन अर्जित करना है।
- ये लोग अनुसंधान के लिये उन जाँचकर्त्ताओं को धनराशि स्वीकृत करते हैं जो उन्हें रिश्वत देने लिये तैयार हैं।
- अधिकारियों की अवहेलना: भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी के बारे में नकारात्मक बातें कर लोग उसकी अवहेलना करने लगते हैं। अवहेलना के कारण अधिकारी के प्रति अविश्वास पैदा होता है और परिणामस्वरूप निम्न श्रेणी के अधिकारी भी उच्च श्रेणी के अधिकारियों का अनादर करेगा, इसी क्रम में वह भी उसके आदेशों का पालन नहीं करता है।
- प्रशासकों के प्रति सम्मान की कमी: राष्ट्र के प्रशासक जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के प्रति जनता के सम्मान में कमी आती है। सामाजिक जीवन में सम्मान मुख्य मानदंड है।
- सरकारों के प्रति विश्वास की कमी: जनता अपने जीवन स्तर में सुधार और नेता के सम्मान की इच्छा के साथ चुनाव के दौरान मतदान के लिये जाते हैं। यदि राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वह लोगों का विश्वास खो देगा और वे ऐसे नेताओं का निर्वाचित नहीं करेंगे।
- भ्रष्टाचार से जुड़े पदों में शामिल होने से परहेज: ईमानदार और मेहनती लोग भ्रष्ट समझे जाने वाले विशेष पदों के प्रति घृणा करने लगते हैं।
- विदेशी निवेश में कमी: सरकारी निकायों में भ्रष्टाचार के कारण कई विदेशी निवेशक विकासशील देशों में निवेश करने से कतराते हैं।
- विकास में देरी: एक अधिकारी जिसे परियोजनाओं या उद्योगों के लिये मंज़ूरी प्रदान करनी होती है, वह धनार्जन और अन्य गैरकानूनी ढंग से लाभ कमाने के उद्देश्य से जान-बूझ कर इस प्रक्रिया में देरी करता है।
- इससे निवेश, उद्योगों की शुरुआत और विकास की गति धीमी हो जाती है।
- यदि उचित सड़क, पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र में कंपनियांँ नए उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती हैं, जो उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में बाधा डालती है।
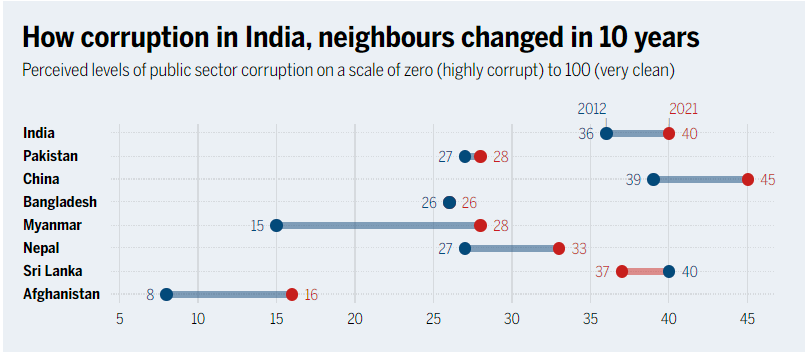
भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने को कानूनी और नियामक ढाँचे:
- कानूनी ढाँचा:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये दंड का प्रावधान है।
- वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधनकिया गया, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने और रिश्वत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।
- लोकपाल तथा लोकायुक्तअधिनियम, 2013 ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है।
- ये "लोकपाल तथा लोकायुक्त" कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
- 1964 में संशोधन: IPC के तहत 'लोक सेवक' तथा 'आपराधिक कदाचार' की परिभाषा का विस्तार किया गया और एक लोक सेवक के लिये आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने को अपराध बना दिया गया।
भ्रष्टाचार को रोकने में नैतिकता का महत्त्व:
- नैतिक सीमाएँ स्थापित करना: नैतिक सिद्धांत सही और गलत को परिभाषित करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में नैतिकता स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करती है, जो स्वीकार्य व्यवहार को अनैतिक या भ्रष्ट आचरण से अलग करती है।
- जवाबदेही को बढ़ावा देना: नैतिकता की मांग है कि व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों की ज़िम्मेदारी लें। जब लोगों को नैतिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो उनके कार्यों के पारदर्शी और जवाबदेह होने की अधिक संभावना होती है, जिससे भ्रष्टाचार, जो कि दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है, की संभावना कम हो जाती है ।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देना:पारदर्शिता एक प्रमुख नैतिक सिद्धांत है। नैतिक संगठनों और व्यक्तियों के पारदर्शी पर और ईमानदारी से काम करने की अधिक संभावना होती है तथा ऐसे माहौल में भ्रष्टाचार का पनपना मुश्किल हो जाता है जहाँ कार्य और निर्णय जाँच के अधीन होते हैं।
- विश्वास कायम करना: विश्वास नैतिक व्यवहार की आधारशिला है। जब व्यक्तियों और संस्थानों को भरोसेमंद माना जाता है, तो उनके भ्रष्टाचार में शामिल होने या उसे बर्दाश्त करने की संभावना कम होती है। समाज में उच्च स्तर का विश्वास भ्रष्टाचार के प्रति प्रलोभन को कम करता है।
- नागरिकों के सद्गुणों को प्रोत्साहित करना: नैतिक मूल्य नागरिक सद्गुणों को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्तियों को दूसरों की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ हासिल करने के बजाय समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। नागरिक सद्गुण भ्रष्टाचार का एक प्रभावशाली निवारक है।
- कानून के शासन का समर्थन: नैतिक व्यवहार कानून के शासन और कानूनी तथा नियामक ढाँचे के प्रति सम्मान को कायम रखता है। भ्रष्ट आचरण में अक्सर कानून को दरकिनार करना या उसका उल्लंघन करना शामिल होता है एवं नैतिकता का पालन कानूनी मानदंडों के प्रति सम्मान को मज़बूत करता है।
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण: नैतिक संगठन और सरकारें भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसिलब्लोअर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। नैतिक मूल्य अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिये प्रोत्साहित करते हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करने एवं संबोधित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- वैश्विक प्रतिष्ठा: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये नैतिक व्यवहार आवश्यक है। नैतिक शासन और निम्न भ्रष्टाचार स्तर वाले देश में विदेशी निवेश और सहयोग की संभावना अधिक होती है।
- दीर्घकालिक स्थिरता: भ्रष्ट आचरण अक्सर अल्पकालिक लाभ प्रदान करता है लेकिन दीर्घकाल में नुकसान पहुँचा सकता है। समाज के सतत् विकास और समृद्धि के लिये नैतिक व्यवहार आवश्यक है।
सार्वजनिक जीवन के मानक और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर नोलन समिति की सिफारिशें:
1995 में यूनाइटेड किंगडम में नोलन समिति ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये सार्वजनिक पदाधिकारियों, अधिकारियों, सिविल सेवकों, नौकरशाहों, नागरिक समाज और नागरिकों द्वारा शामिल किये जाने वाले सात नैतिक मूल्यों की रूपरेखा तैयार की:
- निःस्वार्थता: सार्वजनिक अधिकारियों/नौकरशाहों को लोकहित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये।
- सत्यनिष्ठा: नौकरशाहों को ऐसे किसी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के तहत नहीं होना चाहिये जिससे उनके आधिकारिक कर्त्तव्य प्रभावित हों।
- वस्तुनिष्ठता: सार्वजनिक कामकाज़, नियुक्तियाँ करने, अनुबंध या पुरस्कार और लाभ के लिये लोगों की सिफारिश करने में नौकरशाहों को योग्यता को आधार बनाना चाहिये।
- जवाबदेहिता: नौकरशाह अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं तथा उन्हें अपने पद को भी जाँच/समीक्षा के अधीन रखना चाहिये।
- खुलापन: नौकरशाहों के सभी निर्णयों और कार्यों में खुलापन होना चाहिये। उन्हें अपने निर्णयों का स्पष्ट कारण देना चाहिये तथा सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिये जब व्यापक जन-हित के लिये आवश्यक हो।
- ईमानदारी: नौकरशाह का यह दायित्व है कि वह सार्वजनिक कर्त्तव्यों से संबंधित अपने निजी हितों की घोषणा करे और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाए जो सार्वजनिक हितों की रक्षा करने में बाधक हो।
- नेतृत्व: नौकरशाहों को अपने नेतृत्व द्वारा उदाहरण पेश करते हुए इन सिद्धांतों को विकसित करने के साथ इनका समर्थन करना चाहिये।
भ्रष्टाचार से निपटने हेतु दूसरे ARC की सिफारिशें:
भारत में एक सलाहकार निकाय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय ARC) ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को संबोधित करने और सार्वजनिक प्रशासन की अखंडता तथा दक्षता में सुधार के लिये कई व्यापक सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना एवं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना है। द्वितीय ARC द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मज़बूत बनाना:
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 : दूसरे ARC ने व्हिसलब्लोअर्स के लिये सुरक्षा और प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की। इसमें उन्हें उत्पीड़न से बचाना तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC):दूसरे ARC ने CVC को अधिक स्वतंत्रता, संसाधन और अधिकार देकर भ्रष्टाचार को रोकने तथा मुकाबला करने में उसकी भूमिका को मज़बूत करने की सिफारिश की।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI): आयोग ने भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने में CBI की स्वायत्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाए।
- मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP): द्वितीय ARC ने अधिकारियों की विवेकाधिकार शक्तियों को कम करने के लिये सरकारी प्रक्रियाओं और सेवाओं हेतु स्पष्ट SOP के विकास की सिफारिश की। इससे भ्रष्टाचार एवं मनमाने निर्णय लेने की गुंजाइश कम हो जाती है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का लाभ उठाकर सरकारी लेन-देन में मानवीय हस्तक्षेप और विवेकाधिकार को कम किया जा सकता है। आयोग ने भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित किया।
- पुलिस की जवाबदेही: आयोग ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की अखंडता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये व्यापक पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसमें पुलिस बल में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा व्यावसायिकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
- सामुदायिक पुलिसिंग: सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने से पुलिस और जनता के बीच विश्वास पैदा हो सकता है, जिससे भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में कमी आएगी।
- आचार संहिता: आयोग ने नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये एक आचार संहिता के विकास की सिफारिश की।
- सिटीज़न चार्टर: सरकारी विभागों को सिटीज़न चार्टर अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से जवाबदेही बढ़ सकती है और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हो सकता है।
- मीडिया और शिक्षा: आयोग ने भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों तथा नैतिक आचरण के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग करने का सुझाव दिया।
- संसदीय समितियाँ: सरकारी संचालन और व्यय की जाँच में संसदीय समितियों की भूमिका को मज़बूत करने से भ्रष्टाचार का पता लगाने तथा उसे रोकने में मदद मिल सकती है।
- डिजिटल परिवर्तन: द्वितीय ARC ने मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिये सरकारी प्रक्रियाओं के व्यापक डिजिटल परिवर्तन की सिफारिश की।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न
प्रश्न. 'बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT अधिनियम)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)
- किसी संपत्ति लेन-देन को बेनामी लेन-देन नहीं माना जाता है यदि संपत्ति के मालिक लेन-देन से अवगत नहीं है।
- बेनामी संपत्तियाँ सरकार द्वारा अधिकृत की जा सकती हैं।
- अधिनियम में जाँच के लिये तीन प्राधिकरणों का प्रावधान है लेकिन किसी भी अपीलीय तंत्र का प्रावधान नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) केवल 2 और 3प्रश्न. चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (2021)
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये दंड का प्रावधान है।
- सेवाओं में गुणवत्ता की कमी: भ्रष्टाचार वाली प्रणाली में सेवा की कोई गुणवत्ता नहीं होती है।